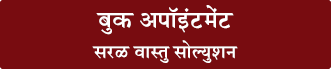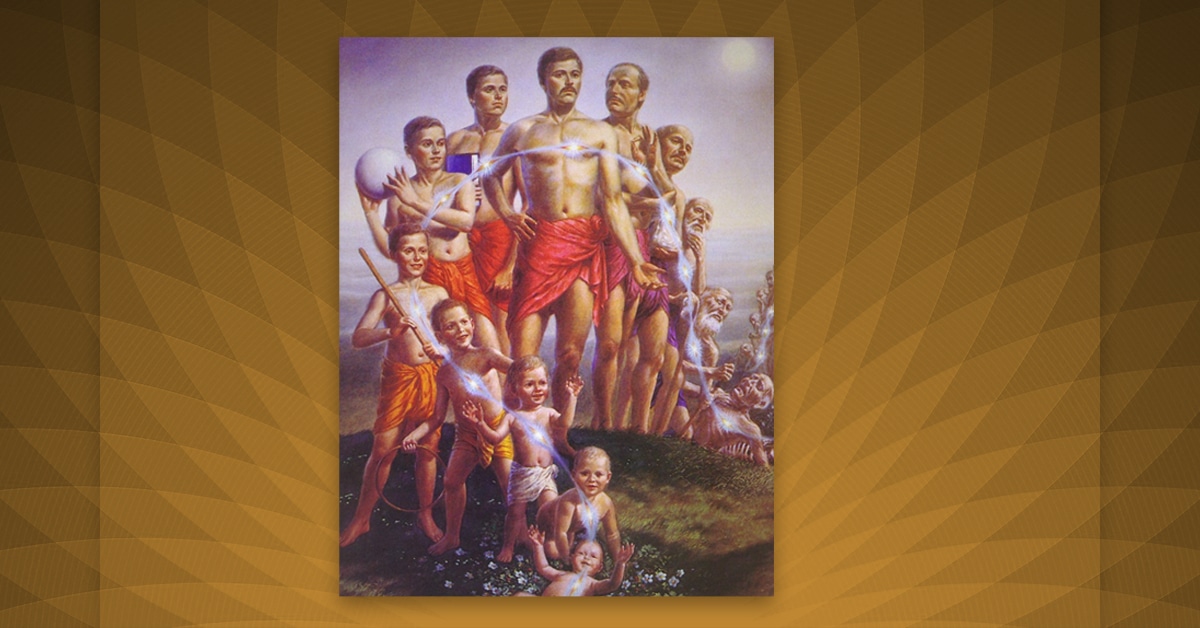वर्तमान में वास्तु के सिद्धांतों तथा तथ्योें के प्रचार एवं प्रसार के लिए बहुत विभिन्न प्रकार के प्रयास किए जा रहेें हैैं। वास्तु के संदेश को घर-घर पहुँचाने के लिए मीडिया की भूमिका बहुत ही अहम हो जाती हैैं; खासकर आजकल के परिप्रेक्ष्य मेें, सोशल-मीडिया मेें वास्तु के बारे मेें इतना ज्ञान एवं जागरुकता व्याप्त हैैं कि लोगोें के मन मेें, वास्तु के प्र्रित कौतुहल जगना अत्यंत ही स्वाभाविक है। परन्तु इतनी सारी जानकारी एवं ज्ञान के भंडार ने, सहज ही लोगो के मन मेें जागरुकता के साथ ही, संशय की भी स्थिति का निर्माण किया है, जिससे अकारण ही लोगों के मन मेें वास्तु को पूर्ण अपनाने तथा दैनिक जीवन में लागू करने को लेकर, काफी सारी भ्रन्तियोें को जन्म दिया है। अतः मुझे यह लगता है कि वास्तु के प्रित लोगों के मन में शक तथा असुरक्षा की भावना का जन्म लेने का मुख्य कारण उनके पास सही तथा वास्तविक जानकारी का अभाव है। बहुत सारे वास्तु-विशेषज्ञोें तथा वास्तु-शास्त्रियों ने यह खतरनाक डरानेवाली भ्रन्ति फैला रखी है कि यदि भवन-निर्माण प्रक्रिया के दौरान अथवा शुरु से ही यदि वास्तु-नियमोें तथा सिद्धांतो की अनदेखी की गई हैैं या नियम तोड़े गए हैैं तो इसके भयानक परिणामस्वरूप, घर के ऊपर घोर विपत्ति तथा मृत्यु के बादल मंडराने लगते हैं, जिससे पूरे परिवार के उपर इसका बूरा प्रभाव पडत़ा है। आजकल बा]जार मेें ‘वास्तु से संबंधित पुस्तके, सी.डी, इन्टरनेट, यू-ट्यूब, सोशल मीडिया आदि पर बहुत अधिक मात्रा मे उपलब्ध है। विभिन्न चेनल्स पर वास्तु से संबंधित जानकारी देने वाले ‘मास्टर-विशेषज्ञोें’ की भरमार हैैं, जिन्हेें स्वयं भी सिविल इंजीनियरिंग, भवन-निर्माण, कला व स्थापत्य कला तथा सामान्य इंजीनियरिंग के बारे मेें न तो कोई जानकारी हैैं और न ही इन्हें इस विषय के मूलभूत सिद्धांतों की कोई समझ होती हैं। आज के यह लोग आधुनिक स्थापत्य कला की डिजाईनोें के साथ, किसी भी प्रकार के समन्वय व रिश्ता कायम करने मेें असमर्थ हैैं।
ऐसे बहुत सारे उदाहरणों, विभिन्न मामलों मेें हमें यह दिखाई देता हैैं कि, पढ़े-लिखे, शिक्षित एवं सुसंस्कृत लोग, अच्छी तनख्वाह तथा अच्छी पद-प्रतिष्ठा होने के बावजूद, इन पाखंडियोें के प्रपंच मेें फँसते ही रहते हैैं। धीरे-धीरे इन लोगों की भावनाओंसे खेलते हुए उन लोगों को अपने बातोें के मायाजाल मेें उलझाकर, अपना उल्लू सीधा करते हुए अपना गोरख धंधा चलाते हैैं। ऐसे तथाकथित विशेषज्ञ सिर्फ अपने स्वार्थ की परिपूर्ति हेतू अत्यधिक लालसा व लालच मेें डूबकर, अपने-अपने यजमानोें को परस्पर विरोधी राय देते रहते हैैं, एवं वास्तु-सुधारों के नाम पर व्यर्थ की तोड़-फोड़ व फेरबदल करवाकर उनसे बहुत अधिक मात्रा मेें पैसे ऐंठते हैैं।
इस प्रकार से अवैध तरीकों से असामाजिक तत्वों की तरह, सिर्फ नाम के यह विशेषज्ञ बातोें की ‘मीठी छुरी चलाकर’ लोगोें को बेवकूफ बनाने के लिए, चंद पैसो के लिए अपनी जमीर व आत्मा को तो बेचते ही हैैं, साथ ही साथ भारतीय वास्तु के सुनहरे नाम के ऊपर कालिख पोंतने का भी घृणित कार्य कर रहे हैैं। ऐसे लोग सच्चे वास्तु-पंडितों के नाम को डूबाने के साथ-साथ उन्हेें बदनाम भी कर रहेें हैैं। परिणामस्वरुप लोगोें के मन मेें वास्तु के प्रित अविश्वास तथा ऐसे तथाकथित वास्तु-पंडितोें के प्रित अवमानना तथा तिरस्कार की भावना का जन्म होता है तथा ‘सही, सहज, असली व सरल-वास्तु विशेषज्ञोें को भी लोग तथा जनसामान्य एक शक जैसे धोखेबाज, टोपी पहनानेवाले तथा धूर्त समझते हैैं। आधुनिक वास्तु नियमों के अनुसार, किचन दक्षिण-पूर्व में तथा पूजा घर उत्तर-पूर्व दिशा में होना चाहिये घर के मालिक का शयन-कक्ष दक्षिण-पश्चिम, खुला स्थान उत्तर-पश्चिम तथा घर का प्रमुख द्वार, या तो उत्तर दिशा मेें या तो पूर्व दिशा मेें स्थित होने चाहिए। स्नानघर, शौचालय अथवा घर के बोर-वेल (चापा कल / कुँए) की दिशा उत्तर-पूर्व मेें नहीं होनी चाहिए। अगर हम इन नियमोें तथा कानूनोें को मानकर नही चलते हैैं, तो ऐसे निर्माण को वास्तु के हिसाब से अशुभ ही माना जाएगा। जब हम अपना इतिहास देखते हैं तो यह पाते हैैं कि हमारे पूर्वजों के रहनेवाले मकान, बिल्कुल भी आज के वास्तु-सिद्धांतों से मेल नहीं खाते हैैं। लेकिन फिर भी वह तथा उनका संयुक्त परिवार कई वर्षोे से एक ही मकान मेें रहते आ रहेें हैैं, सफलता के साथ। उस जमाने की सबसे बड़ी खासियत यह थी कि आज-कल की तरह या वास्तु के नाम से कोई ‘अंधा प्यार या अंधा नशा’ नहीं था, जैसा कि, आज आधुनिक काल में अकसर देखने को मिलता है। यहाँ पर यह बात शाश्वत सत्य है कि, प्रचीनकाल से हमारे पूर्वजोें के रहने के साधन व उपायों मेें, कही भी वास्तु-समतुल्य भवन या वास्तु-उपयुक्त गृहोें का कोई भी वर्णन नहीं हैैं।
इसके बावजूद हमारे पूर्वज हमसे भी कहीं ज्यादा खुश, सुखी, समृद्ध थे, शान्ति तथा स्फूर्ति की सकारात्मक भावनाओें से भरे हुए, सुख और समृद्धि के साथ अपना नित्य जीवन बिताते थे, जोकि, आज-कल की भाग-दौड भरी जिन्दगी से कहीं ज्यादा उत्पादक तथा सकारात्मक था। आजकल की हमारी वर्तमान पीढी, जो बहुत ऊँचे-ऊँचे सपने देखती हैैं, अच्छी तनख्वाह कमाती हैैं तथा सारी सुख सुविधाओंसे सम्पन्न आधुनिक मकानों मेें रहते हैैं, लेकिन अपार धन-संपदा एकत्रित करने के बावजूद भी, अनेकों प्रकार के आधुनिक व्यसनोें से भरपूर ‘लाईफ-स्टाईल’ के कारण बीमारियों एवं रोगों से ग्रिसत रहते हैैं।
अति-व्यस्तता से भरपूर आधुनिक जीवन-शैली, व्यक्ति को बीमार, लाचार, आलसी तथा शारीरिक व मानसिकरूप से पिड़ित बना देती है, यदि ऐसा व्यक्ति परिवार का मुखिया हो या कमाई करनेवाला हो तो फिर घर के हालात और भी खराब हो जाते हैं। यहा पर हम देखते हैैं कि आज के परिपेक्ष मेें मात्र बीस-बाईस अथवा तीस-चालीस साल के उम्र वाले व्यक्तियोें की असमय आधुनिक जीवन शैली घातक बीमारी मेें ही मृत्यु हो जाती हैैं, दिल का दौरा पडऩे से, अकस्मात, आपघात से या आधुनिककाल की क्लिष्ठ जीवन शैली से संबंधित रोगों से।
पुरातनकाल से, हमारे पूर्वज संयुकत परिवार में रहते आये हैं इसके बावजूद उन्हेें आज के परिवारोें के सदस्योें की तरह, आधुनिक जीवनशैली संबंधित रोग जैसे कि, मधुमेह (डायबिटीज़), रक्त-चाप (ब्लड़-प्रेशर), उच्च रक्त-चाप / हाईपरटेन्शन आदि से संबंधित रोग होते ही नहीं थे जो आजकल के महानगरोें की व्यस्त जीवनशैली मेें सामान्यरुप से जाने जाते हैं। पुरातन काल मेें लोगोें की औसत आयु ९०-१०० के बीच तथा बहुत बार उससे भी ज्यादा हुआ करती थी, वर्तमान काल मेें औसत व्यक्तिगत आयु, घटकर मात्र ४०-४५ वर्ष ही रह गई हैैं। जबकि लोग हँसकर यह बात कह देते हैैं कि, हमारे बड़े-बूजुर्ग शुद्ध देशी घी से बना खाना खाते थे इसलिए दीर्घायु हुआ करते थे। ध्यान देनेवाली बात यह हैैं कि, उनकी लम्बी आयु का रा]ज, बिना किसी ‘वास्तु’ आदि का ख्याल कर, बनाए गए घरोें मेें रहने से मिलता है।
हमें जबकि वास्तु आदि के द्वारा बनाए गए निर्मित भवनोें मेें रहनेवाले अकारण ही मृत्यु को प्रप्त होते रहते हैैं या घर के अन्य सदस्य किसी न किसी बीमारी से जूझ रहेें होते हैैं। क्या यह वाकई मेें, एक विडंबना नहीं हैैं? जो आज हमेें साक्षात् देखने को मिलता है। इन्हीं सब उपरोक्त उदाहरणोें से, यह महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है कि, सही अर्थों में वास्तु है क्या? इसका जवाब भी प्रश्न की तरह ही बिलकुल सीधा है वास्तु ज़िंदग़ी जीने की वह ऐसी कला है, जो इन्सान को एक सफल एवं शान्तिप्रिय जीवन पद्धति के साथ, एक सुर एवं एक ताल मेें बाँधकर सहज ढंग से जीने की शिक्षा प्रदान करती है, यह किसी भी एक व्यक्ति के जन्म तथा मृत्यु के साथ संबंधित नही है, और न ही इसको मानकर चलती है कि, व्यक्ति के पास उसके स्वामित्ववाला निजी मकान ही हो।
आज अवश्यकता इस बात की है कि वास्तु के बारे में गलत भ्रंतियों को हटाकर वास्तु के सच्चे स्वरुप को दुनिया के सामने लाया जाये। विश्व-इतिहास, खासकर युरोपियन इतिहास सुशोभित हैैं ग्रीक सभ्यता व संस्कृति से, जिसने ‘ग्रीक-रोमन’ स्थापत्य कला को जन्म दिया है साथ ही सिन्धु-घाटी की सभ्यता, जिसने ‘हडप़्पा तथा मोहेंजोदड़ो व लोथल’ से प्रभावित होकर आधुनिक काल के ‘जल निकासी एवं नालियोें वनहरोें’ (ड्रेनेज-सिस्टम) द्वारा पानी को घर-घर तक पहुँचाने का बीज बोया। इसी प्रकार मुगलकालीन शासन द्वारा प्रभावित सभ्यता ने, ‘मुगलकालीन स्थापत्य व भवन-निर्माण कला’ की नीRव रखी। आज विश्व की हरएक सभ्यता का अपना एक अलग इतिहास व पहचान है, जिन्होंने स्थापत्य व भवन निर्माण कला मेें एक नया आयाम स्थापित किया हैैं। आज इन्हीं सब स्थापत्य कला के उदाहरण हम भवन-निर्माण कला के उत्कृष्ट आधुनिक निर्माणोें मेें देखते हैैं।
परन्तु इन सबसे एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण प्रश्न यह उठता है कि, हम कैसे स्थापत्य कला को किस प्रकार से परिभाषित करें। अंग्रेजी शब्दकोश के हिसाब से, स्थापत्य कला की परिभाषा कुछ ऐसी है: ‘वह कला एवं विज्ञान जो भवनोें की रूपरेखा तथा उनके निर्माण के संबंध मेें विस्तृत जानकारी देती हैैं’। ऊपरी तौर पर देखने से यह इर्ट गारे, सिमेेंट, लोहे व बालू का इतिहास बतानेवाली कला है, मगर दूसरे शब्दोें में कहा जाए तो यह डिजाइन की एक प्रक्रिया है, लेकिन वास्तविकता व सत्य, इससे काफी परे है।
जीवन को सामाजिक तौर पर एक व्यवस्थित तरीके से जीने की व्यवस्था; प्रयः पूरे विश्व मेें एक जैसी ही हैैं फिर भी ऐसे समानार्थक गुणोें के होते हुए भी हम, किसी भी एक भवन को दूसरे भवन से, मिलता-जुलता नहीं पाते है। गौर से देखा जाये तो सिर्फ डिज़ाइन मेें ही नहीं बल्कि स्थापत्य कला को किस प्रकार से दर्शाया जाता हैैं, उसमेें भी अन्तर होता है। स्थापत्य कला, ‘साधारण तौर पर भवनोें व मकानों आदि के निर्माण की वह कला है जो एक सभ्य, सुसंस्कृत, यथार्थवादी, कलावादी तथा भावनात्मकता के धरातल पर खरा उतरने वाले समाज की एक अनिवार्य आवश्यकता हैैं।
यदि हम आज देखेेंगे तो यह पायेेंगे कि लगभग इस सभी प्रकार के समाजों मेें जो भवन, स्मारक, गगनचुम्बी इमारतों व भव्य मकानों आदि के निर्माण के तरीकों से भवन निर्माण कर, उसको नया आकार व आयाम देने के लिए जरूरी स्थापत्य तथा स्थापत्य की रूपरेखा बनानेवाले को जिन्हेें आधुनिक युग में ‘आर्किटेक्ट’ भी कहा जाता है, जो बिल्डिंगो के निर्माण की रूपरेखा के साथ-साथ प्रयुक्त ‘नक्शा’ भी बनाते हैैं। किसी भी प्रकार के भवन-निर्माण मेें सरकारी नियम के तहत बिना जरूरी नक्शे या बिना किसी रूपरेखा के, आवश्यक भवन का निर्माण हो पाना असंभव होता है। बिना किसी स्थापत्य कला आर्किटेक्ट आर्ट के मनुष्य, पाषाणयुग से, सदियोें से प्रकृतिक आपदाओंतथा प्रकृति के विभिन्न प्रकार के संकटो से सामना करता ही आ रहा है और इस आधुनिक काल तक उसका संघर्ष जारी हैैं और आज हमारे पास एक अत्यधिक मजबूत व महत्वपूर्ण बचाव का माध्यम है, प्रकृतिक आपदाओें एवं विषमताओें से रक्षा करने का, जोकि, आधुनिक स्थापत्य कला का सबसे जरूरी अंग है। हमारे समाज मेें जो आधुनिक स्थापत्य कला का सबसे ज्यादा आवश्यक अंग हैैं, वह भवन-निर्माण को ध्यान मे रखते हुए आने वाला एक चिह्न के रुप मेें स्थापित, किसी भी सभ्य व सुसंस्कृत समाज एवं प्रितष्ठान के लिए अति आवश्यक हैैं, जिसके अनुसार निर्माण की प्रक्रिया सुचारु रुप से शुरु होकर अंत तक व्यवस्थित चलती हैैं।
वास्तु-शास्त्र विभिन्न प्रकार के स्थापत्योें की रुपरेखा (नक्शे द्वारा), रिहायशी वातावरण का निर्माण करती हैैं जोकि सभी दैहिक, शारीरिक तथा आध्यात्मिक शक्तियोें एवं ऊर्जाओें से एक साथ मिलकर, असरदार साबित होती हैैं। बाहरी तौर से वास्तु व फेंग-शूई के सभी सिद्धांतो मेें समानता दिखती हैैं; फेंग-शूइर् का उद्देश्य भी ऊर्जा के बहाव को संगठित करना है तथा वास्तु की तरह ही, एक ही लय मेें बाँधना हैैं। इसे ‘जीवन-ऊर्जा’ या ‘प्रण’, संस्कृत मेें कहा जाता हैैं जोकि चीनी भाषा के ‘ची’ के ही समकक्ष या बराबर है। यह समानता विस्तृत वर्णन मेें अलग हो जाती हैैं; जैसे कि, ‘एकदम शुभ – दिशा’; विभिन्न वस्तुओें, कमरों, चीजोें आदि के साथ, जिनका इस्तेमाल, सही रख-रखाव आदि भी विस्तृत वर्णन मेें शामिल हो जाता हैैं।
वास्तु-डिजाइन तीन सिद्धांतों के ऊपर आधारित, पूरे परिसर को समाहित करनेवाली होती है। पहले सिद्धांत को हम ‘भोगाद्यम्’ कहते हैैं, जिसके द्वारा डिजाइन किया हुआ परिसर इस्तेमाल-लायक रहता हैैं और सहज ही इस्तेमाल किया जा सकता है। दूसरे को हम ‘सुख-दर्शन’ कहते हैैं, जहाँ पर डिजाइन किया हुआ परिसर, ‘आँखो को सुहाना लगता है या लगना चाहिए’। इस्तेमाल मेें प्रयुक्त माल तथा जगह का अनुपात, अंदुरुनी एवं बाहरी भाग (आभूषित, रंगत, खिडक़ियोें के साईज व आकार, बिल्डिंग के दरवाजे, कमरे तथा प्रक्षेपण-लय व ताल) सुंदर होने चाहिए। तिसरे सिद्धांत मेें ‘रम्य’ हैैं, ऐसे परिसर द्वारा उसके निवासियों के लिए सुख और समृद्धि के आह्वान को बल मिलना चाहिये।
वास्तु वह प्रचीन व पुरातन वैदिक विज्ञान है, जोकि ‘पर्यावरणीय परमानंद’ से जुड़ा हुआ है, जिसमेें कुछ निर्धारित नियमोें व कानूनोें तथा मापदण्ड़ों को अपनाया गया है। इन मापदण्ड़ों एवं मानकों का निर्धारण एवं निर्माण, काफी लम्बे संघर्ष शोध व प्रयोग द्वारा किया गया हैैं। हमारे पुरातन व प्रचीन भारतीय मंदिरोें तथा ऐतिहासिक इमारतों आदि इन्हीं सब प्रयोगों के ज्वलन्त उदाहरण हैैं। हमारे पास विस्तृत साहित्यिक, पुरातात्त्विक तथा ऐतिहासिक तथ्यों से संबंधित प्रमाणोें से, इन प्रयोगोें की वैद्यता तथा इनके समापन के परिणाम जोकि डिजाइनिंग के तीन सिद्धांतोें के ऊपर आधारित हैैं।
यहाँ पर मैैं, आपको ‘भरत के नाट्यशास्त्र’ का उदाहरण देना चाहूँगा, जो करीबन दो हज़ार साल पुराना हैैं। इसके द्वारा ‘भरत’ ने सिर्फ ‘रंगमंच अथवा नाटक’ की रचना व निर्माण की ही बात नहीं कही गई हैैं, वरन ‘नाट्य आधारित, प्रयुक्त वाद्य-यंत्रोें के सिद्धांत’ का भी वर्णन किया गया हैैं। भरत ने खासकर दो कारण बतायेें हैैं, इस चीज़ पर कि क्योें जरूरी हैैं कि नाटक की समयसीमा तीस मिनटोें से अधिक ना हो। इसका कारण यह है कि सर्वप्रथम यह एक ‘असरदार गूँज’ का सृजन करेगी एवं दर्शकोें के लिए नाटक के पात्रोें को सुनना मुश्किल हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि, सभागृह या नाट्यगृह मेें आखिरी पंक्ति मेें बैठेें हुए दर्शकोें को, मंच के ऊपर नाट्यपात्रोें को देख पाना व उनके चेहरोें के हाव-भावोें को समझ पाना अथवा कलाकारोें के शारीरिक हाव-भाव का अवलोकन कर पाना, प्रयः असंभव ही हो जाता हैैं।
अंत में, ‘भरत’ अपनी अमूल्य राय देते हैैं कि, नाट्यगृह अथवा थियेटरगृह संभवतः गुम्बद की शक्ल मेें अथवा गुफा के रूप में होने चाहिए, जिससे कि एकदम पीछे अथवा दूर बैठे हुए दर्शकोें तक भी कलाकारों की आवाज़ पहुँच सके तथा वह भी नाटक का आनंद उठा सके।