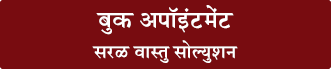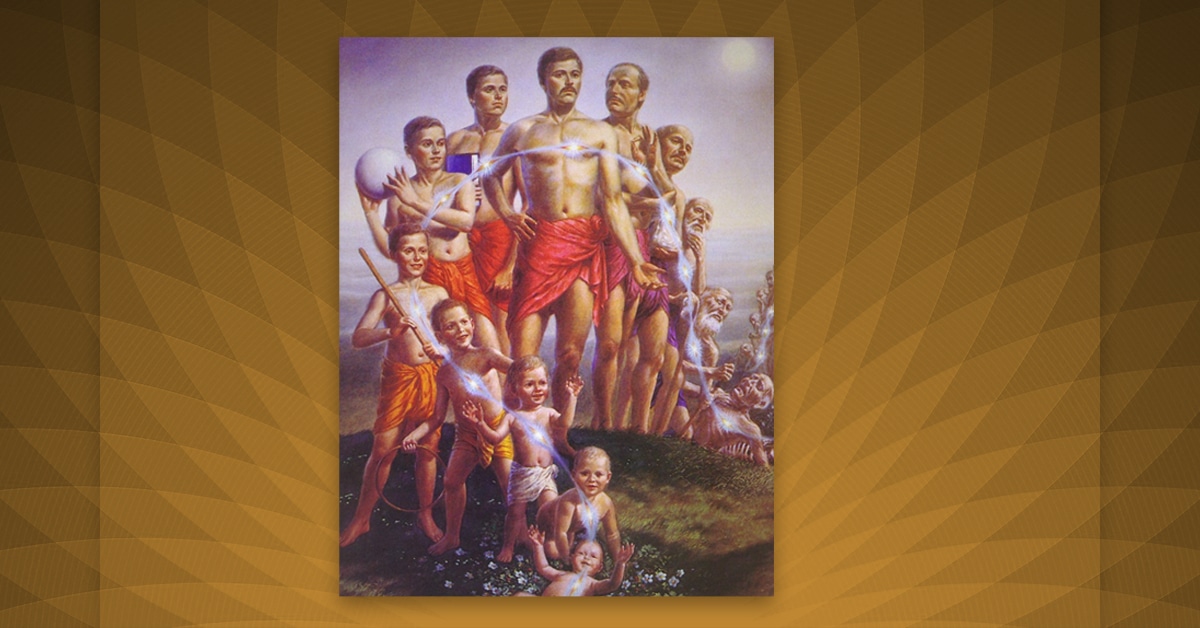सरल शब्द यानि कि समझने व अपनाने लायक सहज सामान्य क्रिया अथवा विशेषता हैैं। इसी प्रकार सरल वास्तु एक कला एवं विज्ञान हैं, जोकि वास्तु-सिद्धांतो को, एक सरल व सहज तरीके से अपनाने का रास्ता दिखलाता है। यह एक सबसे ‘पृथक व विशिष्ट वैज्ञानिक विधि’ है जो हमारे पूर्वजों द्वारा सदियों से इस्तेमाल की जा रही है। जब हम ‘वर्षक्रमिक इतिहास’ के गहरे अध्ययन में जाते हैैं, तो हमें विभिन्न प्रकार की परम्पराओं एवं रस्मों-रिवाजों से अवगत होते हैं जोकि भारतवर्ष मेें प्रचीन-काल से चले आ रहें हैैं। प्रचीन वैदिक व पौराणिक काल व सभ्यता से लेकर आजतक के आधुनिक युग तक, लगभग ५००० (पाँच हजार) वर्षों से ऐसे रीति-रिवाजों, कर्म-काण्डो तथा परम्पराओें की भरमार हमारे इतिहास में उपस्थित रही हैैं।
१. प्रचीन सभ्यता में निहित, हम कुछ ‘आचार-विचार’ स्वरूप छोटी-छोटी चीजों का ख्याल रखते ही आए हैैं, उदाहरण स्वरुप, जब हम किसी दूसरे व्यक्ति या व्यक्तियों से मिलने उनके घर जाते हैैं तो अपने जूते-चप्पल इत्यादि बाहर ही छोड़ देते हैैं। इस रीति का प्रमुख कारण जिनके घर में हम आए हैैं, उनके प्रति हमारे सुसंस्कार, शिष्टाचार, हमारी विनम्रता तथा दूसरोें का सम्मान करने की भारतीय प्रवृत्ति व परम्परा का हम निर्वाह करते हैैं। इसके अलावा घर के स्वामी के प्रित सम्मान व्यक्त करने का भी यह हमारा एक तरीका है। इसी प्रकार विशेषकर, जब हम किसी धार्मिक या तीर्थस्थान के दर्शनों के लिए जाते हैैं तो मंदिर आदि में प्रवेश करने से पहले, हम अपने जूते-चप्पल तथा पादुकाएँ इत्यादि, नियत स्थान पर या धार्मिक स्थल के बाहर ही रखकर अंदर प्रवेश करते हैं। फिर चाहें वह धार्मिक स्थल कोई मंदिर, गुरुद्वारा या मस्जिद, चर्च-गिरजाघर, मजार, मकबरे, समाधि या अन्य किसी भी प्रकार का धार्मिक स्थल से संबंधित हो; उसकी पवित्रता को बनायें रखने के लिए यह अत्यंत जरुरी हैैं कि, हम उन सभी नियम कानून का पालन करें जो किसी भी धार्मिक स्थान में प्रवेश के लिए जरुरी होते हैं।
विज्ञान के अनुसार भी गंदे जूते, चप्पल अंदर पहनकर आने से सब प्रकार के कीटाणु व विषाणु इत्यादि का घर के अंदर प्रवेश करने का खतरा हो जाता हैैं जिससे गंदगी के साथ-साथ सभी प्रकार के नकारात्मक ऊर्जाओं का भी पूरे घर अथवा कार्यस्थल में अधिपत्य हो जाता हैैं। जिस वजह से पूरे घर मेें नकारात्मक तथा निराशावादी वातावरण का सृजन होता है, जो पूरे घर को प्रदूषित तो करता ही है साथ ही साथ अंदर विद्यमान सकारात्मक ऊर्जा व घनात्मक शक्ति को काफी हद तक कम व प्रयः विलुप्त ही कर देता है।
२. दूसरों के प्रित अपनी श्रद्धा, इज्जत व सम्मान प्रदर्शित करने के लिए अथवा दूसरों से मिलने पर अपनी खुशी व्यक्त करना, पूर्वी व दक्षिणी एशिया के ज़्यादातर देशों में काफी समय से होता आ रहा हैैं तथा यह प्रथा आज भी अत्यंत प्रचलित है। थाईलैण्ड़, कम्बोडिया, वियतनाम, इंडोनेशिया, श्रीलंका, सेचेल्स, मालदीव व मोरिशियस इत्यादि दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में, हाथों को जोड़कर, ‘नमस्कार’ की मुद्र में या खासकर जापान जैसे देशों में झुकने की परंपरा हैैं ।
भारतवर्ष में हम अपनी दोनों हथेलियों को नमस्कार की मुद्र में जोड़कर, लोगों का स्वागत करते हैैं, जब अतिथि हमारे घर पधारते हैं। इस मुद्र के पीछे यह मंशा व तात्पर्य होता हैैं कि में विनित ढंग से आपके समक्ष नतमस्तक हूँ। जब हम लोग थोड़ा झुककर, दोनों हाथों को नमस्कार की मुद्रा में जोडत़े हैैं तो इसके पीछे का उद्देश्य यह होता है कि, हम अपने हृदय की आंतरिक शुभेच्छा व खुशी का इ]जहार दूसरोें से कर सके। सबसे महत्वपूर्ण बात हम अपने आस्तित्व को भुल ही जाते हैं जब हम दूसरों के सामने नतमस्तक होते हैैं। अहंकार न करना व दूसरों के समक्ष झुकना हमारे ‘जमीनी-धरातल’ पर रहने का द्योतक हैैं जो हमारे अंदर की ‘मैैं’ की भावना का दमन करता हैैं जो हमारी प्रचीन भारतीय संस्कृति व सभ्यता की एक महत्त्वपूर्ण विशेषता हैैं। इसके अलावा भी, ‘नमस्ते या नमस्कार’ मुद्र का शाब्दिक अर्थ यह है कि आगंतुक अथवा अतिथि के साथ हमारा दिल जुड़ रहा है। दोनों हाथों की हथेलियों को परस्पर जोडऩा, ”अंजलि-मुद्र“ कहलाती हैैं।
‘सर को नीचे झुकाना’ हमारे अंदर के प्यार, स्नेह, जोश व रिश्तों की गरमी को तथा समाज के अन्य सदस्यों के प्रित, हमारी ‘समर्पण भावना’ को भी दर्शाता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, नमस्कार की मुद्रा में दोनों हथेलियों को पास लाने का यह औचित्य हैं कि हम अपने ऊर्जा प्रवाह में उपयुक्त रक्त-धमनियों को परस्पर जोडक़र, संपूर्ण शरीर में ऊर्जा के प्रवाह, फैलाव व आदानप्रदान को शरीर के अलावा बाहर निकलने से रोकना है। इससे हमारे सभी ‘सत्कर्मोे का संचय’ होना भी हैैं। जब हम एक-दूसरे को परस्पर नमस्कार करते हैैं, तो हम पाते हैैं कि हमारे शरीर के ऊर्जा- स्रोतों से, ऊर्जा-प्रवाह बलपूर्वक आगे बढ़कर, एक-दूसरे में समाहित होते हुए, अपने पथ पर अग्रसर होता जाता हैं। नमस्कार की मुद्र में हमारी हाथों की कोहनियों की स्थिति भी एक विशिष्ट प्रकार की ‘यौगिक मुद्र’ धारण करती हैैं जो लम्बे समय पश्चात् हमारे मनुष्य शरीर को स्वस्थ, सुड़ौल व शारीरिक सौष्ठव मेें वृद्धि करती हैैं।
३. माथे पर ‘तिलक’ धारण करना, हमारे धार्मिक चिह्नें का प्रितक है, जो ‘शिवजी के तीसरे नेत्र’ अथवा ‘ज्ञान नेत्र’ का द्योतक है। लाल कुमकुम, श्वेत चंदन अथवा रक्त चंदन के तिलक का लेप धारण किए हुए व्यक्ति की ओर सबका ध्यान आकर्षित होता है। इसी तरह दोनो भृकुटियों के बीच यानि उपज्ञाचक्र पर लम्बा तिलक अथवा बिन्दी को नाक से ऊपर धारण करने वाले व्यक्ति के व्यक्तित्व में स्वत: निरवार आने लगता है। इसी प्रकार से भारतीय स्त्रियों के माथे पर परम्परागत ढंग से धारण की जाने वाली विभिन्न प्रकार की बिन्दियाँ, साधारण से साधारण स्त्री की सुंदरता में भी चार-चाँद लगा देती हैैं। विभिन्न आकार, रंग व प्रकार की बिन्दियाँ, सिन्दूर से भी ब्याहता या सुहागिन स्त्री के माँग का टीका अथवा साधारण सिन्दूर की बिन्दी अथवा कुमकुम लगाना, भारतीय स्त्रियों की प्राचीन युग से, विश्व-प्रिसद्ध परम्परा रही हैैं। जो स्त्री-विशेष के ‘प्रकृतिक-सौन्दर्य’ को बढाने के साथ-साथ, उनके लालित्व व स्त्री-सुलभ कोमलता व कमनियता को प्रदर्शित करने का एक अत्यंत ही लोकप्रिय तरीका रहा है हमारे वेद, पुराणों एवं धार्मिक ग्रंथो में भी सौन्दर्य- प्रसाधनों में बिन्दी व सिन्दूर लगाने का भी उल्लेख मिलता है।
आज्ञा चक्र को चेतना का आसन कहा जा सकता है। कहने को तो चेतना नरव से शिखा तक होती है लेकिन बैठती आज्ञाचक्र पर है, इसलिए जब किसी व्यक्ति का ध्यान गहरा हो जाये यानि आत्मचिंतन बढे और उसकी चेतना उर्ध्वगामी होने लगे तो समझना चाहिए कि आज्ञा चक्र तरंगित हो रहा है।
योगशास्त्र के अनुसार, माथे पर दोनों भौहों के मिलने के स्थान पर, जो बिन्दु होता हैैं, उसे ”आज्ञा-चक्र“ कहते हैैं जोकि एक ‘जाल’ के जैसा होता है यह ”कुण्डलिनी के सर्प-शक्ति“ के साथ, मेरुदण्ड के आधारभूत केन्द्र से पैदा होकर, ”मूलधारा“ के रूप में शीश या मस्तिष्क तक पहुँचता है। समाधिस्थ होने की स्थिति को प्रप्त करने के लिए साँस को संयत कर, दोनों भौहों के बीच ‘तिलक’ लगाने की जगह पर ध्यान केन्द्रित कर, दिमाग को नियंत्रित करना पडत़ा हैैं। इस प्रक्रिया द्वारा ध्यानावस्था या ध्यानमग्नता के सर्वोेच्च शिखर तक पहुँचा जा सकता हैैं। इस पूर्ण ‘भावावेश’ की स्थिति को,’मानसिक भावावेश’ की सर्वोत्तम ध्यानमग्न अवस्था को प्रप्त करना कहते हैैं, जोकि मनुष्य जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य मोक्ष को प्रप्त करना है। इस ‘भावावेशिक ध्यानमग्नता की चरम उत्तम अवस्था में, प्रयः श्वसन-क्रिया लगभग रुक जाती हैैं, नाड़ी-स्पंदन क्षीण हो जाति है तथा मनुष्य निर्जिव हो जाता है। ऐसी परमावस्था को प्रप्त करने के लिए वैदिक-काल से, ऋषि-मुनि वर्षों तक, घोर तपस्या व यज्ञ आदि करते रहे हैैं। तांत्रिक योग व कापालिक तथा औघड़ क्रिया के रुप में समझी जानेवाली इस क्रिया को कर्म-काण्ड के अनुसार एक महत्वपूर्ण संज्ञा दी गई है। अंततोगत्वा यह क्रिया, साँस लेने, रोकने एवं हमारे हृदयगति व नाड़ी के स्पंदन को नियंत्रित करने की अभूतपूर्व क्षमता है जो बहुत ज़्यादा व नियमित अभ्यास के द्वारा ही, संभव है।
महिलाओं में खासकर महाराष्ट्र प्रदेश में, किसी भी शुभ अवसर पर या किसी सार्वजनिक समारोंह में ‘हल्दी-कुम्कुम’ परम्परा का निर्वाह लगभग अनिवार्य सा ही होता है। इसके अलावा, ‘लाली’ अथवा सुर्ख लाल रंग, एक राजस व समृद्ध सकारात्मक ऊर्जा की निशानी होती है तथा सुहागिन स्त्रियों के लिए, उनके सुहाग या पति की रक्षा हेतु, निभाने वाली एक अति-महत्वपूर्ण ‘हिन्दू-धर्मनीति व रीति’ हैैं।
४. भारतवर्ष में बचपन में बच्चों के ‘नाक-कान’ छिदवाने की परम्परा प्रचीन काल से ही चली आ रही है। इसके पीछे एक धार्मिक मान्यता व धार्मिक परम्परा भी जुड़ी हुई है। राजाओं, सामन्तों, व्यवसायिकों व समाज के अन्य वर्गोर् तथा वर्णों के लोगों में, कान छिदवाने की परम्परा वर्षो से चली आ रही हैैं। सौन्दर्य व भारतीय परिपाटी के अंतर्गत, महिलाओं में विभिन्न प्रकार के नाक व कान के आभूषण नथनी व नथनियाँ, टिकली व टियारा, झुमके आदि धारण करने का चलन हैैं,। विभिन्न धर्मों व समुदायों मेें, शादी-विवाह इत्यादि में, परम्परागत भारी व जड़ाऊ गहनों को धारण करने की परम्परागत प्रथा है।
आज भी राजस्थान खासकर वहां के गाँव व कस्बों में रहने वाले लोग बचपन से ही अपने बच्चों के कान छिदवाते हैैं। राजपूत वंश के लोगों के यहाँ यह प्रथा खासकर आज भी प्रचलित हैैं। ब्रह्मणों, क्षत्रियोें, बनिया आदि वर्णों में बचपन से बच्चों के कान छिदवाने की प्रथा प्रचलित है। पूरे देश भर में लडक़ियों व स्त्रियों की स्त्री-सुलभ कोमलता व सौन्दर्य को दर्शाने के लिए, शैशव-काल में ही दोनों कान छिदवा दिए जाते हैैं। विवाह के समय दुल्हन को कानों में बड़ेबड़े झुमके तथा नाक मेें व]जनदार भारी सोने की नथनियाँ आदि धारण करना, विवाह के रस्मोंरिवाजों में अभिन्न रुप से शामिल हैैं एवं वंश-परम्परा को निभाते हुए दादी-नानी से मिली अमूल्य धरोहर गहनों को पहनने की परम्परा आज भी यथावत कायम है।
आधुनिक काल में भारतवर्ष की परम्पराओं व रीति-रिवा]जों की देखा-देखी, वर्तमान फैशन की प्रवृत्तियों में नवयुवकों व नवयुवतियों के द्वारा विश्वभर में, नाक, कान, भौहों, होठों आदि शरीर के विभिन्न अंगो पर व स्थानों पर छिद्र करवाकर सोने व चाँदी के विभिन्न प्रकार के आभूषणों को धारण करने की जैसे प्रथा ही चल पड़ी है। भारतीय सौन्दर्य के विश्व-प्रिसद्ध होने का इससे उत्कृष्ट उदाहरण हो ही नही सकता है जो हमारे लिए गर्व की बात है।
इस परम्परा के पीछे एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी है। औषधि-विज्ञान व आधुनिक चिकित्सा विज्ञान के द्वारा ‘नाक-कान छेदन’ करवाने से देखने, सुनने की क्षमता एवं साँस लेने की क्रिया में अभूतपूर्व वृद्धि होती है। आज-कल ‘शरीर में गोदनाँ’ व ‘शरीर में विभिन्न स्थानोें पर छिद्र करवाना’, दोनों ही बहुत प्रचलित व अनुकरणीय, विश्वभर में व्याप्त ‘शारीरिक कला की आधुनिकतम प्रवृत्तियाँ’ हैं। आज ज़्यादा से ज़्यादा लोग भौतिकवादी व उपभोक्तावादी प्रवृत्तियों के शिकार होते जा रहें हैैं तथा स्वर्ण-आभूषणों के ऊपर अत्यधिक मात्रा में खर्च करके महंगे से महंगे आभूषण पहनते हैं एवं स्त्रियों द्वारा गहने व आभूषण, उदाहरणार्थ – नाक, कान, गले, माथे, मांग, हाथोें-पैरों, कमर, पैर व हाथ की अंगुलिओं में आभूषणों को धारण करना, आजकल महंगा शौक बनता ही जा रहा हैैं। अपनी मान्यता अनुसार सभी त्यौहार, शादी-ब्याह या अन्य समारोह, खास दिनों पर जैसे ‘अक्षय-तृतीया, दीपावली, धनतेरस के शुभदिन पर आभूषण खरीदने की परम्परा आज भी सदियों से हमारे भारतीय समाज में चली आ रही है, जो ]ज्यादातर लोगों के लिए अपने पैसे व शान का प्रदर्शन करने का सुअवसर होता हैं।
५. लोगों का यह विश्वास हैैं कि ‘ब्रह्म-मुर्हुत’ (प्रतः ४ बजे से ५.३० बजे तक), हिन्दू-शास्त्रों व पुराणों के अनुसार बहुत ही शुभ समय होता हैैं; आध्यात्मिक व आध्यात्म से संबंधित क्रियाएँं, जिनमें मुख्यतः ‘वेद, पुराण, शास्त्र एवं विभिन्न पवित्र धर्मग्रंथो का पठन, मनन व चिंता करना सर्वथा अनुकूल रहता है। पुरातनकाल के गुरुकुल से लेकर आज के शिक्षण संस्थानों तक, ४ वेदों (ऋगवेद, सामवेद, यर्जुवेद, अथर्ववेद) का पठन व मनन प्रतः काल की मधुर-वेला में ही उत्तम तरीके से स्मरण रखते हुए ही होता आ रहा हैैं। यह समय विद्यार्थियों के लिए ध्यान केन्द्रित कर, याद रखने का सर्वोत्तम समय है।
योगासन व विभिन्न प्रकार के यौगिक आसन प्रतःकाल में ही किए जाते हैैं, जिससे हमारा शरीर व मन तरोता]जा हो जाते हैैं तथा हमारी आत्मिक शक्ति भी सशक्त हो जाति है। आज की व्यस्त दिनचर्या के लिए, विभिन्न प्रकार की ‘ध्यान मुद्रओं व ध्यान लगाने’ की विधिओें द्वारा हमारा दिमाग व मस्तिष्क ‘धारदार’ होता है एवं इन क्रियाओं को करने से हमारी ‘बैद्धिक शक्ति’ (विवेक व क्षमता) का विकास भी होता है। हमारे मस्तिष्क की क्षमता में भी अप्रत्याशित वृद्धि होती हैैं। व्यायाम से भी हमें यही सब लाभ मिलते हैैं। आयुर्वेद के अनुसार ब्रह्म मुर्हुत मेें, समस्त वातावरण का वायुमंडल चँद्रमा के सकारात्मक ऊर्जा से नवजागृत हो उठता है तथा वनस्पतियों, पेड़-पौधों आदि के द्वारा प्रणदायी ऑक्सिजन बनाया जाता है। यह ताजा ऑक्सिजन (प्राणवायु), सभी मनुष्यों के स्वास्थ्य को सुधारने का प्रयत्न करती है। इस समय को ‘अमृत-वेला’ या वेल भी कहा जाता हैं जिसका अभिप्रय ‘अमरत्व का जीवन-अमृत’ हैैं। इस समय हवा में तंदुरुस्ती-४१… ऑक्सिजन, ५५…नाईट्रोजन की मात्रा होती है तथा कार्बन-डाईऑक्साइड की मात्रा सिर्फ ४… ही होती हैैं।
इसलिए इस समय का अधिक से अधिक इस्तेमाल हमारी ज़िंदगी की ‘बैटरी को रिचार्जर्’ करने में लगाना चाहिए। सूर्योदय के उपरान्त, मनुष्य अपनी नित्य क्रियाओं में लिप्त हो जाते हैैं तथा निरन्तर बढ़ते हुए समय के साथ-साथ शान्ति भंग होने लगती हैैं जिसके फलस्वरुप ध्यान-केन्द्रित कर, आध्यात्मिक क्रिया या आध्यात्म पर सोचना असम्भव-सा हो जाता है।
६. पूजा स्वरुप लोग ‘पुष्पांजलि’ देवी-देवताओं को समर्पित करते हैैं। पुष्प के गुणों का आकलन करना, सूर्य को दीपक दिखाने के बराबर हैं। जन्म से लेकर मृत्यु तक, पुष्प भारतीय परम्पराओं व कर्म-काण्डों के अभिन्न व अद्वितीय अंग रहे हैैं। पुष्प-सज्जा, पुष्प-मालायें, पुष्प-तोरण, गजरें इत्यादि में पुष्प की उपयोगिता प्रचीनकाल से अब तक त्योहारों के दौरान पुष्पों की रंगोली, समारोंहों में पुष्प-गुच्छ देने की परम्परा, पुष्प की लडिय़ों द्वारा विभिन्न अवसरों पर सज्जा, प्रतिष्ठानों व संस्थानों में सांस्कृतिक कार्यक्रमों के दौरान मंच-सज्जा आदि के मुख्य साधन हमेशा से, पुष्प-पत्तियाँ व डालियाँं इत्यादि रही हैैं।
प्रतीक पुष्पों द्वारा हम निरन्तर चलते रहनेवाले सृजनात्मकता, उर्वरता, प्रजनन तथा बीज से पेड़ बनने की प्रक्रिया का अवलोकन करते हैैं तथा इसे एक प्रतिक के रुप में भी देखा जाता है। पूजा, समर्पण की भावना, ईश्वर के प्रित विश्वास व प्रर्थना, भगवान से वरदान की कामना आदि मनोकामनाओं द्वारा, अपने मन की मुराद पूरी करने हेतु, पुष्प की अधिकाधिक उपयोगिता मनुष्य की अभिलाषा पूरी करने में ही प्रयुक्त होती हैैं। पुष्प द्वारा पुष्पांजलि का अर्पण करने की विधि जनसमुदाय द्वारा नवरात्रि या दुर्गा-पूजा आदि के दौरान अनिवार्य मानी जाति है। सभी समुदायों के लिए पूजा व अन्य धार्मिक अवसरों पर देवी-देवताओं के ऊपर पुष्प-न्यौछावर करने से, पूजन का महत्त्व बढ़ जाता हैैं। पुष्प का महत्त्व, पुरातन-काल से आधुनिक-काल तक तथा आगे आनेवाले चिरन्तन युगों तक, हमेशा यूँ ही बना रहेगा।
७. जल लेकर पुजारी द्वारा आचमन विधि करना या करवाना, पूजा के दौरान, स्वयं तथा यजमान के द्वारा पूजाविधि करवाना किसी भी धार्मिक अनुष्ठान एवं पूजा का अभिन्न अंग होता है। आचमन क्रिया के बिना कोई भी पूजा विधि, किसी भी प्रकार से आरंभ ही नही होती है। आचमन क्रिया के दौरान हम अपनी अंजुली मेें जल लेकर पीते हैैं तथा मस्तिक की चारों दिशाओं में घुमाते हुए, जल को छिडक़ते हैैं। इसके पश्चात ही विधिवत पूजा का प्रारम्भ होता है। इसके अलावा प्रितदिन प्रतःकाल एक लोटे में जल लेकर, सूर्य देवता के समक्ष पूर्व दिशा में अथवा बरगद के पेड़ के सामने, जल आचमन या जल-प्रच्छेदन विधि करना, बहुत सारे भारतीयों का पूरे देशभर में
नित्यप्रित क्रिया हैैं जिसका नियमपूर्वक स्त्री व पुरुष पालन करते हैैं। सूर्य-भगवान को साक्षी मानकर, प्रतःकाल स्नान करने के पश्चात् शुद्ध होकर आचमन की विधि करके दिन का शुभारंभ करना प्रयः हिन्दू धर्म के सभी अनुयायी कभी न कभी जरुर पालन करते हैैं।
आयुर्वेेद के अनुसार अंजुली में जल लेकर पीना अत्यंत चिकित्सा विज्ञान व वैज्ञानिक तर्क यह बताता है कि जब हम धीरे-धीरे अंजुली में लेकर पानी पीते हैैं तो हमारे मुँह मेें लार उत्पन्न करने की क्षमता व मात्रा बढ़ जाती हैैं, जिससे अधिक मात्रा में उत्पन्न लार से भोजन पचाने में आसानी होती है तथा यह हमारी शरीर की पाचनक्रिया में भी सहायक बनती है, जब हम हमारे खाने को चबाते हैैं तब खासकर सख्त भोजन को नरम करने व पचाने लायक, मुँह में ही बना देता हैैं।
८. जब शिष्यों एवं विद्यार्थियों द्वारा सामूहिक रुप से श्लोक मंत्र, दोहों, वेदों का एक साथ उच्चारण किया जाता है, तो ‘उत्पादित ध्वनि-तरंगो’ से गोलाकार आकृति में परस्पर ध्वनि-तरंगो का फैलाव, एक सकारात्मक अति-उत्तम वातावरण को जन्म देता है।
ध्वनि-तरंगे जब किसी भी तरल पदार्थ के संपर्क में आती हैैं अथवा जब किसी द्रव्य या तरल पदार्थ को देवी-देवताओं की मूर्तियों पर चढ़ाया जाता हैैं तो, इस प्रकार से मूर्तियों पर गिरनेवाले तरल-पदार्थ काफी ज़्यादा प्रभावित होकर, सकारात्मक ऊर्जा के रुप में परिणित हो जाता है तथा यही द्रव्य या तरल पदार्थ, पवित्रता का स्रोत भी हो जाता है। जब यह तरल पदार्थ किसी भी प्रकार के पत्थर या धातु के संपर्क में आते हैैं तब इसी प्रकार विभिन्न द्रव्य-पदार्थ अलगअलग शक्तियोें की तीव्रता से भर जाते हैैं, उदाहरणार्थ, पीतल या ताँबा के बर्तन जो काफी फायदेमंद होते हैैं। इनमें रखा हुआ चरणामृत या जल भक्तों में बाँटा जाए, तो लोगों को एक अपूर्व आनंद देनेवाले स्वाद का प्रसाद प्रप्त होता है। इसके अलावा सामान्य स्वास्थ्य के हिसाब से भी ऐसे बर्तनों में रखा भोज्य पदार्थ पाचन के हिसाब से भी सर्वोेत्तम होता है इस संदर्भ मेें पुराणों वेदो एवं अन्य धार्मिक ग्रंथों मेें भी वर्णन मिलता है, कुछ समय पहले तक हमारे दादा-दादी, नाना-नानी व बुजूर्गोर् द्वारा पीतल, ताँबे व काँसे के बर्तनों का इस्तेमाल किया जाता था, जिससे स्वास्थ्य संबंधी समस्यायें बहुत ही कम उन्हें सताती थी तथा दीर्घायु प्राप्त करते थे। इन पुरानी धातुओें से बने बर्तनों की जगह आज स्टील एवं प्लास्टिक के बने बर्तनों का अत्यधिक झुकाव हैैं। परन्तु प्लास्टिक एवं स्टील के बने बर्तन कभी भी काँसे, पीतल व ताँबे के बर्तनों की बराबरी मनुष्यों के लाभ के परिप्रेक्ष्य में कभी भी नहीं कर सकते हैैं।
९. साधारणतः मासिक-धर्म को निभाती स्त्रियाँ, उन खास दिनों में चिडच़िड़ी हो जाती हैैं तथा अधिकतर नारियों के स्वभाव में मूलभूत परिवर्तन हो जाता हैैं। संयुक्त परिवारों में आज भी मासिक-धर्मवाली स्त्री न तो रसोईघर में प्रवेश कर सकती हैैं और न ही खाना बना सकती हैैं। इसके अलावा धार्मिक अनुष्ठानों व पूजा-अर्चना तथा मंदिर में प्रवेश करना भी ऐसी स्त्रियों के लिए सख्त निषेध रहता हैैं।
मासिक-धर्मवाली स्त्री को अपरोक्ष रुप से परिवार से अलग ऐसा निजी स्थान दिया जाता हैैं, जहाँ पर वह शारीरिक व मानसिक पीड़ा तथा पेट-दर्द से राहत पाने के लिए ज़्यादातर समय आराम करके ही बिताती हैैं। दैनिक गृह-कार्यों से उसे वंचित रखा जाता हैैं एवं घर की दूसरी स्त्रियाँ यह सब कार्य संभालती हैैं। किन्तु, महानगरों मेें रहनेवाले छोटे परिवार के लोग, अपनी जीविका को चलाने के लिए खासकर पति-पत्नी या स्त्री-पुरष दोनोें नौकरी करते हैैं, जिसके कारण उनकी ज़िंदगी बहुत ही ज़्यादा व्यस्त हो जाती हैैं। ऐसी गृहस्थी में, ऐसे कठिन नियम का पालन करना, व्यवहारिक व तर्कसंगत नही रहता है।
सही अर्थ में इन रुिढ़वादी परम्पराओं का संयुक्त परिवारों में आज भी बहुत ज़्यादा महत्त्व हैैं क्योेंकि संयुक्त परिवारों में स्त्रियाँ एक-दूसरे का सहारा बन जाती हैैं, जिससे हर एक महिला को अपने उन पीड़ा भरे दिनों में बारी-बारी से, आराम मिल जाता हैैं तथा बुर्जुग महिलाएँ भी ह इसमें अपनी भागीदारी एवं ज़िम्मेदारी से पीछे नहीं हटती।
वास्तु के हिसाब से भी यह प्रचीन व्यवस्था अत्यंत ही उत्तम, तर्कसंगत तथा वैज्ञानिक नियमानुसार हैैं। इसी प्रकार से प्रचीन भारतीय सभ्यता व संस्कृति के गहन-शोध एवं अध्ययन द्वारा मैैंने इन रीति-रिवाजों के पीछे का महत्त्व एवं इनके वैज्ञानिक दृष्टिकोण को कड़ी मेहनत के बाद सरल-वास्तु के सिद्धांतो व प्रचीनतम वास्तु-शास्त्र के सिद्धांतो के बीच के अंतर को समझ पाया, हालाँकि दोनोें के ही बीच, काफी हद तक तो समानताएँ हैैं।
सरल वास्तु के अंतर्गत आने-वाली विधियाँ सीधी-सादी, व्यवहारिक तथा समझने एवं इस्तेमाल में अत्यधिक आसान हैैं। यह एक पूर्णतः वैज्ञानिक पद्धति के ऊपर आधारित विज्ञान है, जो सकारात्मक ऊर्जा को घर अथवा कार्यस्थल पर ‘संग्रहित तथा संचय’ करता हैैं। इससे संपूर्ण घर एवं घर के सदस्यों में पूर्ण सकारात्मकता से भरे असरदार परिणाम दृष्टिगोचर होते हैैं।
प्रितष्ठानों के लिए भी यह इतना ही असरदार हैं एवं बहुत ही कम समय में, आशा के अनुरुप परिणाम देता हैैं। इस पुस्तक को लिखने व छपवाने का प्रमुख कारण, साधारण व सामान्य मनुष्यों की आवश्यक्ताओंएवं इच्छाओं को पूर्ण करने का एक साहसिक प्रयत्न है, जिससे व्यक्ति एक सफल, शान्तिमय व समृद्धियुक्त जीवन जी सकता है। बहुत सारे विशेषज्ञों ने विभिन्न प्रकार सेकी पुस्तकों के माध्यम से वास्तु विषय से संबंधित, बहुत सारी पुस्तकें लिखी हैैं, जो वास्तु के मनुष्यों के ऊपर असर व उनके इस्तेमाल प्रक्रिया की ओर इशारा करती है। इनसे प्रभावित होकर आमआदमी को वास्तु के नाम पर, पैसा पानी की तरह बहाने के लिए बाध्य होना पडत़ा है। तथा कथित वास्तु विशेषज्ञों द्वारा लिखित पुस्तकों के नियम बता कर वर्तमान या नई खरीदी गयी संपत्ति में अनियांत्रित तोड़-फोड़ और मरम्मत का दवाब बनाया जाता है। यह करने की सीख, इन लोगों को वास्तु के ऊपर बडी मात्रा में देशभर में छपनेवाली, आसानी से उपलब्ध वास्तु-पुस्तकों द्वारा मिलती हैैं। यह सस्ती व भ्रमक पुस्तकें मनुष्यों के मन में परस्पर विरोधाभास, विस्मय तथा उदासीनता व उलझन को जन्म देती हैं।
जनसामान्य द्वारा भविष्य की चिन्ता करते हुए, मेहनत से कमाई हुई संपत्ति, इन पुस्तकों के अंदर लिखे नियमोें व विचारोें को मानने एवं अपने घर व प्रितष्ठान में इनको लागू करवाने के लिए, बाध्य हो जाते है, और इस तरह एक आमआदमी अनायास ही अंधविश्वास के तहत हज़ारों रुपए अपने बर्बाद कर देता है।
इस समस्या का प्रमुख कारण यह है कि आजकल के वास्तु-विशेषज्ञ अपनी-अपनी पुस्तकों द्वारा एक प्रकार के अंधविश्वास व छलावे को बढ़ावा दे रहें हैैं तथा इसके चलते अनियंत्रित खर्चे के कारण गृहस्थों की आर्थिक स्थिति बहुत ही जीर्ण-शीर्ण एवं कमजोर हो जाती हैैं। मकान के मूलभूत ढाँचे मेें वास्तु-पुस्तकों के हिसाब से किए गए परिवर्तन के कारण, आसपास का वातावरण भी प्रभावित होता हैैं तथा परिवार के सदस्यों का जीवन, पूरी तरह से अस्त-व्यस्त हो जाता हैैं। सबसे महत्त्वपूर्ण बात यह है कि इससे घर की मूलभूत नींव में अस्थिरता आ जाती है।
जबकि इसके विपरीत, सरल-वास्तु की राय अनुसार सिद्धान्तों को आत्मसात करके, मकान के ढाँचे में परिवर्तन किए बिना और बगैर किसी तोड़-फोड़ के वास्तु-दोषों के निराकरण एवं वास्तु सुधारों के उद्देश्यों की पूरी तरह पूर्ति की जा सकती है। सरल-वास्तु विधि में सरल-वास्तु से संबंधित, कुछ-एक उपाय ऐसे किये जाते हैैं जो गृहस्वामी के ऊपर खर्चेे के भार को, एकदम कम से कम कर, व्यक्ति-विशेष को आवश्यक वास्तु-सुधार प्रदान किया जाता है तथा उनके जीवन वपरिवार में निर्धारित वास्तु-सुधार, सुख, समृद्धि एवं शान्ति अवश्य ही लेकर आती हैैं। यह बदलाव बहुत ही जरुरी एवं व्यापक होता हैं जो आस-पड़ोस व समाज में व्यक्ति-विशेष की प्रतिष्ठा और गरिमा को बढ़ा देता है। घर के लिए आवश्यक वास्तु-परिवर्तन करना बदलाव के द्वारा ही संभव हो पाता हैैं, जिससे घर में समृद्धि और खुशहाली लौट आती हैैं तथा व्यक्तिविशेष व परिवार दोनों के ही जीवन में आमूल परिवर्तन, निश्चित तौर पर सुखाकारी के लिए ही होता हैैं। यहाँ पर सावधानी बरतनेवाली बात यह है कि, सामान्य व्यक्तियों को इन झूठें, फरेबी किस्म के वास्तुतज्ञों से किस प्रकार बचाया जाए तथा उन्हें वास्तु-दोषों से भी सुरक्षित रखा जाए, जिससे कि जनसामान्य इनके फरेब के जाल में न फँसकर उनके छलावे का शिकार भी न हो।
भविष्य में सरल-वास्तु के ईमानदार एवं कुशल विशेषज्ञों की इन्हीं उपरोक्त कारणों के लिए ही समाज में और भी अधिक आवश्यकता हैैं, जो जनसाधारण में सरल-वास्तु के प्रित अडिग विश्वास जगाने एवं व्याप्त वास्तु संबंधित भ्रन्तियों को दूर करने का प्रयास करेंगे, जिससे इन नकली व धूर्त, सिर्फ नाम के वास्तुतज्ञों का असामाजिक धंधा जो वास्तु के नाम पर हो रहा हैं वह हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा।