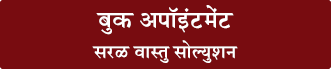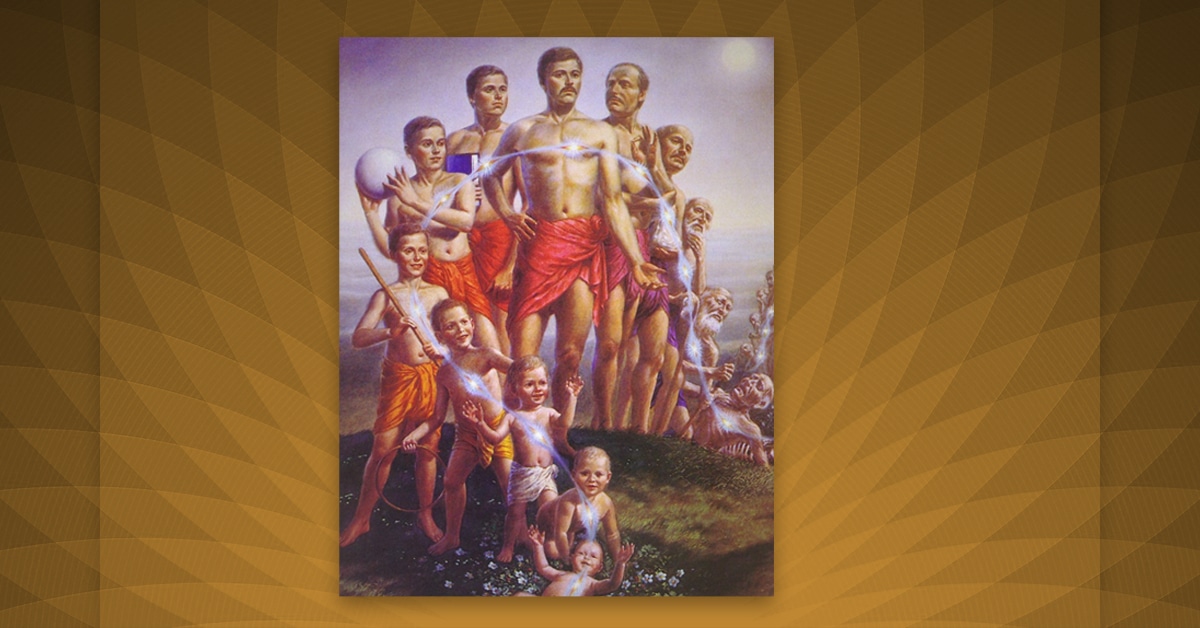जैसे कि, हम सब जानते हैं कि हमारी प्रकृति व वातावरण ऊर्जा से भरे हुए हैं। इस ऊर्जा को हम आगे सकारात्मक व नकारात्मक ऊर्जाओं में विभाजित कर सकते हैं। सरल-वास्तु का अभिप्राय: वातावरण में ‘सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाओं’ को कम करने या पूर्णत हटा देने का ही हैं, जिससे वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा की वृद्धि की जा सके। जिसके द्वारा हम घर-गृहस्ती सरल व सफलतापूर्वक व्यतीत कर सके सरल-वास्तु अपनायें हुए घर में सुख, समृद्धि, शान्ति एवं आनंदमयी वातावरण की, सहज ही उत्पत्ति होती है तथा इन सभी सदस्यें के जीवन में हर्ष, सुसमय तथा सफलता की चाबी, सही समय पर लेकर आती हैं। इन सरल उदाहरणों द्वारा हम अपने घर कार्यस्थल में ऊर्जा के असर से रुबरु होते हैं तथा हमारा सामना सभी प्रकार की सकारात्मक व नकारात्मक ऊर्जाओं से होता ही हैं।
उदाहरण नं. १ – ऐसा देखा गया हैं कि, कभी-कभी जब हम किसी छोटे बच्चे को किसी भी कार्यक्रम जहाँ पर काफी लोग एकत्र होते हैं अथवा किसी पाटी इत्यादि में ले जाते हैं, तो बच्चा उस स्थान पर तो शान्त रहता है, परन्तु घर वापस आने पर चिड-चिड़ाने लगता है तथा कुछ ही क्षणें में अपने आप, रोना भी शुरु कर देता है। जोकि माता-पिता तथा घर के अन्य सदस्यें के पुचकारने एवं मनाने पर भी नही रुकता है। बच्चा लगातार रोता ही चला जाता है तथा बच्चे को चुप कराने के सभी प्रयास, घर के सदस्यें द्वारा, असफल ही साबित होते हैं। जब सभी प्रयास असफल हो जाते हैं तो सबको दादी-माँ व नानी-माँ एवं हमारे पूर्वजों द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला, पुराना रामबाण इलाज याद आ जाता है। हमारी नानी-दादी इत्यादि घर के शिशुओं का लगातार रुप से रोना रुकवाने के लिए, मुट्ठीभर घरेलू नमक अथवा लवण लेकर, तीन बार बच्चे के इर्द-गिर्द एक गोले की शक्ल में घुमाती है। तत्पश्चात्, वह उस मुट्ठीभर नमक को आग के चूल्हे में झोंक देती है, नहें तो बहते हुए पानी में, बहा देती हैं। चमत्कारपूर्ण तरीके से इतना करते ही, बच्चा एकाएक रोना-बिलखना एकदम से बंद करके, चुप हो जाता है। यह परंपरा लगभग पूरे भारत वर्ष में है जो किसी ना किसी रुप मे प्राचीन काल से विघमान है।
अब एक महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठना अत्यंत स्वाभाविक है कि बच्चा सर्वप्रथम फूट-फूटकर रोया ही क्यें तथा उस बच्चे के अलावा किसी भी अन्य वयस्क के उढपर जो पार्टी या समारोह में मौजूद थे, उन लोगों पर कोई असर पड़ा ही नही। ऐसा क्यों हुआ, इसका कारण समझना सामान्य मनुष्य के लिए, बहुत ही मुश्किल है। इसके अलावा दूसरा प्रश्न यह भी उठता हैं कि एक मुट्ठीभर साधारण नमक ही क्यें इस्तेमाल किया गया, कोई दूसरा पदार्थ क्यें नहीं लिया गया! एक और अजीबोगरीब बात नज़र उतारने के दौरान, घर के बड़े-बूढों द्वारा मुट्ठीभर नमक को छिपाकर दूसरें की नज़र बचाकर ही, आग में ही क्यें झेंका गया; उस नमक को किसी कूड़ेदान अथवा बाहर या पानी में क्यों नहीं बहाया गया?
इन सब भारतीय परम्पराओं पर आधारित नज़र उतारने की परम्परा इत्यादि में, आश्चर्यचकित कर देनेवाला तथ्य यह है कि किसी भी प्रकार का शोध इस विषय पर आजतक किसी के भी द्वारा नहीं किया गया है तथा इस प्रकार के अनसुलझे पुराने कर्म-कांडो एवं परम्परा पर आधारित प्रश्नें की जानकारी, हासिल करने का प्रयत्न क्यें नही किया गया! यह परम्पराएँ प्राचीन वैदिक-कालीन युग से चली आ रही हैं। स्पष्ट तरीके से कोई भी विशेषज्ञ, वैज्ञानिक अथवा आचार्य इनको परिभाषित नहीं कर पाये हैं। फिर भी मुझे, तर्कपूर्ण ढंग से इन परम्पराओं के पीछे के उद्देश्यों के बारे में शोध द्वारा किया गया अध्ययन लोगें के सामने स्पष्ट करने का प्रयत्न करना चाहिए।
जैसा सर्वविदित हैं कि, हरएक जगह में सकारात्मक व नकारात्मक शक्तियाँ सक्रिय होती हैं, लेकिन भीड़-भाड़वाली जगह में नकारात्मक शक्तियें की भरमार होती हैं। जब विभिन्न प्रकार की नकारात्मक शक्तियें से भरपूर जगह पर शिशु को ले जाया जाता है तो कुछ समय तक तो वह नकारात्मक ऊर्जा को झेल सकता हैं, परन्तु जल्दी ही इसका असर बच्चें पर निश्चित रुप से पड़ने लगता है, जिसके परिणामस्वरुप वह नकारात्मक शक्तियें से वशीभूत होकर रोना शुरु कर देता है। ऐसे बच्चों की जब हम तुलना करते हैं बड़ो से, जिनके सहने की क्षमता बच्चों से तो बहुत ज़्यादा ही होती हैं। अपनी इस प्रतिरोधक क्षमता के हिसाब से बड़े (वयस्क) नकारात्मक शक्तियें का सामना करते हैं, परन्तु शिशुओं की प्रतिरोधक क्षमता कम होने से नकारात्मक शक्तियों का विरोध बच्चें बहुत ही कम समय तक कर पाते हुए थक-हार जाते हैं एवं लम्बे समय तक नकारात्मक ऊर्जाओं के सान्निध्य में रहने के कारण उनका मिजाज़ चिड़चिड़ा हो जाता हैं जिससे वह रोने लगते हैं।
मुठ्ठीभर नमक को आग में झेंकने का तात्पर्य यह है कि बच्चें के ईर्द-गिर्द की नकारात्मक शक्तिओं को साधारण नमक सोख लेता और नमक में घुली नकारात्मक शक्तिओं को सुलगी हुई आग में इसलिए झेंका जाता हैं कि यह नकारात्मक शक्तियाँ दूसरे मनुष्यों में बच्चें के द्वारा न फैले जिससे अन्य वयस्कों को यह प्रभावित ना कर पाए, जो बच्चें के आसपास मौजूद हो।
उदाहरण नं. २ – सभी मनुष्य कभी न कभी अपनी जिंदगी में, किसी न किसी तीर्थ-यात्रा पर जरुर जाते हैं। भले सालाना तौर पर एक ही बार जाए। ऐसा माना जाता है, कि तीर्थस्थानें पर परिश्रमपूर्वक जाने से, हमारे जीवन से पाप की मात्रा कम होती हैं एवं पवित्रता की मात्रा बढ़ जाती हैं, जो आगे चलकर मोक्ष पाने में सहायक होती हैं।
धार्मिक स्थानें पर जाकर, भगवान अथवा हमारे इष्टदेवों का स्मरण करके, जब हम ध्यानावस्था में बैठते हैं तो हमे एक अपूर्व आनंद का अनुभव होता हैं। ऐसी परमानंद अवस्था में हमे चैतन्य का एहसास होता हैं तथा हमारी आत्मा, परमात्मा से एकाकार होकर मिल जाती हैं। साथ, हमें परम-मोक्ष पाने की दिशा में और यही मिलन की अवस्था हमारी आत्मिक शांन्ति एवं संतुष्टि को बढ़ाने के साथ-साथ हमे परम मोक्ष की दिशा में अग्रसर करती हैं। वाकई में यह एक बड़ा प्रश्नचिह्न है कि क्या भगवान का घर, हमारे घर से बाहर स्थित मंदिर या किसी अन्य धार्मिक जगह पर ही हैं! क्या हमारे घर में हमारे ईश्वर का मिलना असंभव हैं?
आईये अब सरल-वास्तु के माध्यम से इस विषय पर विस्तृत रुप से विचार करें। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारों आदि में ज़्यादातर स्थानों पर पीने के पानी के नलों की व्यवस्था होती हैं। जहाँ भक्त अपने हाथ-पाँव, मुँह, मस्तिष्क आदि को पानी से साफ कर एवं कुल्ला करने के पश्चात् ही शुद्ध व साफ-सुथरे होकर विभिन्न धार्मिक स्थलों के अंदर प्रवेश करते हैं। जल को एक शुद्धिकरण करने के पदार्थ के रुप में देखा जाता है। जल हमारे शरीर में स्थित, तथा आसपास के वातावरण में उपस्थित सभी नकारात्मक शक्तिओं को हटाते हुए वातावरण को, शुद्ध और सकारात्मक बनाता है। जैसे-जैसे भक्तगण शुद्धिकरण के पश्चात पवित्र तनमन से मंदिर में स्थित गर्भ-गृह की ओर बढ़ते हैं, तो पूरा माहौल भक्तिमय हो जाता हैं। भक्तजनें की जयजयकार, बजते हुए ढोल-नगाड़े, घंटे-घड़ियाल, तूति, नादस्वरम, ढाक-ताशा व अन्य वाद्ययंत्रों के साथ मिलकर सकारात्मक ध्वनि-तरंगो की वजह से सकारात्मक ऊर्जाओं का मिलन होता है एवं पूरा वातावरण ही भक्तिमय व पवित्र हो जाता हैं।
यह भक्तिमय वातावरण पूरे तौर से मंदिर के गर्भ-गृह में स्थित नकारात्मक शक्तिओं को नष्ट करता है। इसी प्रकार से, गिरजाघर में ‘आर्गन’ वाद्य-यत्र तथा गिरजे के छत पर स्थित बड़े घन्टे की आवाज़ जो रस्सी के द्वारा नीचे खड़े होकर बजाई जाती है, मस्जिद से मुल्ला द्वारा अजान की आवाज़, गुरुद्वारे से गुरबानी की आवाज़ आदि ध्वनियें से तरंगित भक्तिमय वातावरण, जो घनात्मक व सकारात्मक शक्तिओं द्वारा परिपूर्ण होकर, शोभायमान हो जाता है। इसी प्रकार से ‘पुष्पांजलि’ तथा ‘प्रात व संध्या आरती’, उत्सवों में ‘मध्यरात्रि की महाआरती’ द्वारा मंदिर या किसी धार्मिक स्थान के आसपास के वातावरण में उपस्थित सभी प्रकार की नकारात्मक शक्तियाँ कम हो जाती हैं, जिसके परिणामस्वरुप सकारात्मक शक्तियाँ एरां सकारात्मक प्रवृत्तियाँ खूब बढ़ जाती हैं।
ऐसे सुन्दर वातावरण में, सही मायनो में व्यक्ति को सर्वोत्तम माहौल व मार्गदर्शन मिलता हैं, जिससे वह अपने अंतर्मन में परम्-शान्ति व परम्-सुख का अनुभव करते हैं। आप एक ऐसी अवस्था की कल्पना कीजिए, जब किसी मंदिर अथवा मस्जिद में प्रवेश करने से पहले आपको किसी भी प्रकार का कोई जल-स्रोत न मिले, जिससे कि आप अपने हाथ-पाँव धो सके या वजु कर सके, कोई घन्टा-घड़ियाल न मिले जो बजाया जाये पूजा के दौरान, न तो दीप-दिये जलायें जाये, न आरती की जाये, न कपूर सुलगायी जाये न लोबान, न आरती के लिए घी का दीपदान व न पंचप्रदीप ही जलाकर आरती की जाये, न वातावरण में सुगंधित अगरबत्ती जलाई जाए और न ही इन सबकी मिश्रित सुगंध से सराबोर पवित्र वातावरण में भगवद्भजन किया जाए तो ऐसे अधार्मिक वातावरण मे अधिक मात्रा में नकारात्मकता, उदासीनता तथा निराशावादिता होना स्वभाविक है।
इस तथ्य से यह स्पष्ट हैं कि ऐसे वातावरण का निर्माण करना होगा, जोकि पूजा-पाठ के लिए सर्वथा अनुकूल हो एवं जहाँ भक्ति-भाव से ओत-प्रोत वातावरण हो। यदि ऐसे सकारात्मकता से भरे वातावरण का, हमारे घर व कार्यस्थल में समावेश होगा तो हमारे घर एवं कार्यस्थान में भी सकारात्मक व घनात्मक ऊर्जाओं में अभूतपूर्व बढोत्तरी होगी, ऐसा मुझे परम्-विश्वास है।
एक ऐसा घर जहाँ सभी प्रकार की सकारात्मक, आशावादी ऊर्जाओं से ओत-प्रोत वातावरण का निर्माण होता है, वहाँ अपने-आप ही सभी पारिवारिक सदस्यों का विकास होता है। ‘सरल-वास्तु’ एवं इसके सहज व सरल सिद्धांतों को हम अपने घर, परिवार एवं कार्यस्थल में लागू करके, हम हमेशा ऐसे सकारात्मक वातावरण को बनाए रख सकते हैं।
यहाँ पर मैं उदाहरणस्वरुप, आपको एक घटना के बारे में बताना चाहूँगा जो मेरे साथ घटित हुई, एक समारोह में, जब मैं एक व्याख्यानमाला के अंतर्गत संभाषण दे रहा था। एक मुसलमान बंधु, जो मेरे संभाषण के दौरान उपस्थित थे, उन्होंने सभा के मध्य खड़े होकर, एक अत्यंत ही सहज सवाल किया, ‘गुरुजी, हिन्दूओं में, मंदिरो तथा अन्य धार्मिक स्थलों पर पूजाअर्चना के दौरान घन्टा-घड़ियाल, ढोल-मंजिरे इत्यादि वाद्य-यंत्र बजाने की परम्परा हैं, जबकि मुसलमानों में किसी भी प्रकार के संगीत संबंधित वाद्य अथवा गाना गाने व घन्टे-घड़ियाल इत्यादि का प्रयोग पूर्णत वर्जित हैं चाहे वह किसी समारोह में हो या किसी अन्य जगह पर। नमाज़ पढ़ने के दौरान तो कदापि नहीं। इस्लाम धर्म के नियमानुसार किसी भी प्रकार के संगीत संबधित गानाबजाना, सुनना व चर्चा करना, संगीत वाद्य-यंत्रो को बजाना व सुनना, एक प्रकार से इस्लाम धर्म के अनुयायिओं द्वारा पवित्र कुरान के सिद्धांतो के हिसाब से तथा मुस्लिम धर्म की विभिन्न परम्पराओं के खिलाफ होने के साथ-साथ, ‘हराम’ भी हैं, ऐसी संज्ञा मुसलमानो द्वारा ही दी जाती हैं।“
मेरा उत्तर अत्यंत ही सीधा, सरल तथा स्वाभाविक था। मैंने कहा, ‘मुस्लिम भाईयों को मस्जिदों से अजान के द्वारा संगीतमय सूर में ही, नमाज़ पढ़ने के लिए आमंत्रित किया जाता हैं। पाँच वक्त की नमाज़, मौलाना अथवा मौलवीजी द्वारा पढाई जाती हैं जिसमें ‘अल्लाह हू अकबर’ भी एक खास अंदाज़ व सूर में ही, पूरी जमात द्वारा बोली जाती हैं। इसके अलावा मस्जिदों में प्रवेश करने से पहले व नमाज़ पढने से पहले अपने सर, हाथों, पैरों, मुह व चहरे को धोते हैं व कुल्ला करते हैं जिसे वजू करना कहते हैं। इस प्रकार पवित्र होकर अपने अंदर सकारात्मक ऊर्जा पैदा करते हैं और पंक्तिबद्ध तरीके से नमाज़ पढ़ने की क्रिया आरंभ कर संयुक्त ऊर्जा द्वारा पूरे मस्जिद भर मे एक सकारात्मक व आशावादी वातावरण का निर्माण करते हैं। इस प्रकार से सामूहिक रुप में ‘जुम्मे’ की नमाज़ पढ़ने से सभी नमाज़ियों में परस्पर सकारात्मकता का आदान-प्रदान होता है, यह सत्य है कि सभी नमाज़ियों को, नमाज़ पढ़ने के पश्चात् सब के मन में परम संतुष्टि व शान्ति की भावना जन्म लेती हैं।
अजान मौलवीजी द्वारा ऊँची आवाज़ में एवं एक विशेष प्रकार की सूर व तान में, मस्जिद से लाउढड-स्पीकरों द्वारा दी जाती हैं जो चारों दिशाओं में गुँजायमान होकर प्रतिध्वनित होती हैं। इस गूंज के द्वारा अत्यधिक मात्रा में आवाज़ गूँजती हुई प्रतीत होती हैं, जिससे इन सम्मिलित ध्वनि-तरंगो द्वारा उत्पादित अधिक से अधिक मात्रा में, ‘सकारात्मक व घनात्मक ऊर्जा’ का बहाव शुरु होता हैं जो ‘सकारात्मक प्रार्थनाओंरुपी नमाजों’ में मिलकर, परस्पर ‘सकारात्मक नमाज़ियों’ के रुप में एक, सम्मिलित व सामूहिक प्रार्थना या नमाज़ व खुदा की बंदगी में परिवर्तित होती हैं, मस्जिद तथा आस-पास के वातावरण की सभी सकारात्मक ऊर्जाओं को एकीकृत करने एवं उन्हें बढाने में भी सहायक होती हैं।
इसी प्रकार से ईसाईयों के द्वारा इस्तेमाल किए गए धार्मिक स्थलों जैसे कि, चर्च और गिराजाघरों में बजनेवाले, बड़े-बड़े घन्टे व घडियालों को रस्सी द्वारा नीचे से ही बजाकर, सामूहिक प्रार्थना के लिए बुलाया जाता हैं। इसके अलावा, ‘मदर-मेरी व जिसस् (यीशू मसीह)’ की प्रतिमा के सामने मोमबत्ती व अगरबत्ती जलाना, पुष्पगुच्छ व पुष्पमालाओं को पवित्र मेरी तथा उनकी गोद में स्थित यीशू (ईसा) मसीह की मूर्तियों पर माला अर्पन करना बहुत ही पवित्र और नेक कार्य समझा जाता हैं, चर्च के बाहर व चर्च में ‘अल्टर’ के सामने नियत जगह पर व संगीतमय ‘आर्गन’ का बजाया जाना खासकर इतवार के दिन; सामूहिक रुप से एक पवित्रता एवं सकारात्मक से भरी ऊर्जा से संचारित वातावरण की सृष्टि करता हैं, जो चर्च में आनेवाले सभी भक्तों को आंतरिक आनंद, शान्ति व अपूर्व सुख का अनुभव करता है।
सरल-वास्तु के अनुसार, एक खास लय व ताल में कर्तलध्वनि करना या ताली बजाना, एक प्रकार से सर्वेच्च उदाहरण हैं, व्यक्ति-विशेष की सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने के लिए; जैसे कि जब हम गणेशजी की आरती करते समय सामूहिक रुप से ताली बजाते हैं तो आरती के भजन व स्वरों में स्पंदित, ‘सुखकर्ता दुःखहर्ता वार्ता विघ्नाची…’ सभी भक्तगण भावावेश में आकर एक सूर व ताल में तालियाँ बजाते चलते हैं, जिससे उन्हें हृदय के अंदर, परमसुख व नवचेतना एवं नवस्फूर्ति का अनुभव होता जाता हैं। इसी प्रकार से जब किसी नाटक, चलचित्र (सिनेमा) अथवा सर्कस के कलाकारों की कलाओं को देखकर हम उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए ज़ोर ज़ोर से तालियाँ बजाते हैं, खासकर जब हम किसी खेल के मैदान या स्टेडियम में खिलाड़ियों को अच्छा खेलता हुआ देखते हैं तो अनायास ही जोर-जोर से ताली बजाने का जी करता हैं एवं हम अपने आपको रोक नहीं पाते हैं। कभी-कभी तो ऐसा होता हैं कि क्रिकेट जैसे खेल में, बल्लेबाज द्वारा चौका या छक्का मारने पर, हम तालियाँ बजाते ही रहते हैं, इसलिए यह प्रश्न करना भी उचित है कि इस स्वाभाविक क्रिया के पीछे का राज एवं वैज्ञानिक तर्क क्या है!
वास्तु के अनुसार जब हम ताली बजाते हैं, तो उस खास जगह में उपस्थित सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाएँ लगभग विलुप्त सी हो जाती हैं अथवा उनमें अत्यधिक कमी हो जाती हैं। जब असंख्य लोग एक साथ ताली बजाते हैं तो उनके सामूहिक कर्तलध्वनि द्वारा उत्पन्न सम्मिलित ध्वनि का असर चौगुना होकर, चौगुने रुप से सकारात्मक ऊर्जा वातावरण में समावेश करती हैं। वातावरण में अत्यधिक मात्रा में सकारात्मक ऊर्जाओं की असर के कारण खिलाड़ियों व कलाकारों के चैतन्य में सात-चक्रों का नवजागरण होता हैं, जिसके परिणामस्वरुप उनके अंदर शारीरिक व मानसिक रुप से सकारात्मकता का पुन संचार होता हैं, इसलिए ही वह दर्शकों के समक्ष अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने को उत्साहित होते हैं। इसके पीछे का वैज्ञानिक तथ्य यह कहता हैं, कि उनके मस्तिष्क की ग्रंथियों से और भी ज़्यादा मात्रा में ‘टेस्टेस्ट्रोन’रुपी रसायन का स्राव होता हैं, जिससे इनके शरीर व मन में स्फूर्ति में इज़ाफा होता हैं तथा दिमाग के शक्तिवर्धन के लिए एवं अलग परिस्थितियों में कामोत्तेजना को बढाने के लिए एक शक्तिवर्धक दवा का भी काम करता हैं।
यही सब वास्तव में, वैज्ञानिक रीति से, स्वतहोनेवाले वास्तु-सिद्धान्तों का हमारे मनुष्य जीवन में पूर्ण समावेश व आत्मसात् करने की हमारी प्रवृत्ति को भी दर्शाता हैं।